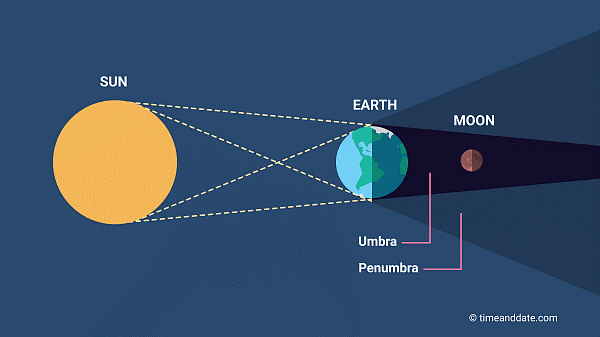Q 1.हाल ही में समाचारों में रहा ‘आयरन डोम’ निम्न में से क्या है?
- डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन
- नेविगेशन सिस्टम
- एयर डिफेंस सिस्टम
- फेसिअल रेकग्निशन ट्रैकिंग (FRT) प्रणाली
ANSWER: 3
- आयरन डोम एक मोबाइल ऑल-वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है।
- प्रणाली को कम दूरी के रॉकेट को रोकने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Q 2.बायोहब पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक पहल है जो विश्व स्तर पर प्रयोगशालाओं और भागीदारों के बीच वायरस और अन्य रोगजनकों के तेजी से साझाकरण को बढ़ाने के लिए है।
- स्विट्ज़रलैंड के स्पीज़ में पहली डब्ल्यूएचओ बायोहब सुविधा स्थापित की जाएगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और स्विस परिसंघ ने हाल ही में डब्ल्यूएचओ बायोहब सिस्टम के हिस्से के रूप में पहली डब्ल्यूएचओ बायोहब सुविधा शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।
- डब्ल्यूएचओ बायोहब सिस्टम के तहत स्पीज़, स्विट्जरलैंड में स्थापित सुविधा वैश्विक स्तर पर प्रयोगशालाओं और भागीदारों के बीच वायरस और अन्य रोगजनकों के तेजी से साझाकरण को बढ़ाएगी।
- जोखिम मूल्यांकन को सूचित करने और इन रोगजनकों के खिलाफ वैश्विक तैयारी को बनाए रखने के लिए अन्य प्रयोगशालाओं में वितरण के लिए जैविक सामग्री की सुरक्षित प्राप्ति, अनुक्रमण, भंडारण और तैयारी के लिए यह सुविधा केंद्र के रूप में काम करेगी।
पृष्ठभूमि
- वर्तमान में, अधिकांश रोगजनक साझाकरण देशों के बीच द्विपक्षीय रूप से और तदर्थ आधार पर किया जाता है, जो धीमा हो सकता है, और कुछ देशों को लाभ और उपकरणों तक पहुंच के बिना छोड़ सकता है।
बायो हब सिस्टम
- इस मुद्दे को हल करने के लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने नवंबर 2020 में बायोहब सिस्टम की स्थापना की है।
- यह सदस्य राज्यों को जैव सुरक्षा, जैव सुरक्षा और अन्य लागू नियमों सहित पूर्व-सहमत शर्तों के तहत बायोहब के साथ और उसके माध्यम से जैविक सामग्री साझा करने में सक्षम करेगा।
- यह प्रतिक्रिया गतिविधियों में समयबद्धता और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करेगा।
Q 3.कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह कोयला मंत्रालय का एक प्रस्तावित मिशन है जो खेत में पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करता है और थर्मल पावर उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है।
- इसका उद्देश्य सह-फायरिंग के स्तर को वर्तमान 5% से उच्च स्तर तक बढ़ाना है ताकि थर्मल पावर प्लांटों से कार्बन न्यूट्रल बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा हो सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 2
- विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन
- यह खेत में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करेगा और थर्मल पावर उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करेगा।
- यह देश में ऊर्जा संक्रमण और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के हमारे लक्ष्यों का और समर्थन करेगा।
- बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) में भी योगदान देगा।
मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:
- सह-फायरिंग के स्तर को वर्तमान 5% से बढ़ाकर उच्च स्तर तक करना ताकि ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन न्यूट्रल बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा हो सके।
- बायोमास छर्रों में सिलिका, क्षार की अधिक मात्रा को संभालने के लिए बॉयलर डिजाइन में अनुसंधान एवं विकास गतिविधि करना।
- बायोमास पेलेट्स और कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करने और बिजली संयंत्रों तक इसके परिवहन की सुविधा के लिए बायोमास को-फायरिंग में नियामक मुद्दों पर विचार करना।
Q 4.राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अकादमी, जिसका अक्सर समाचारों में उल्लेख किया जाता है कहाँ स्थित है?
- दिल्ली
- मुंबई
- पुरी
- नागपुर
ANSWER: 4
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अकादमी, नागपुर में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) में निदेशक के एक पद के सृजन के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अकादमी की स्थापना वर्ष 2018 में नागपुर में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज (एनसीडीसी) के साथ विलय करके की गई थी।
- अकादमी का मुख्य परिसर निर्माणाधीन है, तब तक यह एनसीडीसी के मौजूदा परिसर से कार्य कर रहा है।
- अकादमी वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) / राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) / नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करती है और इसकी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित होने की परिकल्पना की गई है।
- यह SAARC और अन्य देशों के आपदा प्रतिक्रिया कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
- निदेशक, एनडीआरएफ अकादमी के पद के निर्माण के साथ, संगठन की कमान और नियंत्रण एक वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी को सौंपी जाएगी, जो इच्छित उद्देश्यों के अनुसार संस्था का संचालन कर सकता है।
Q 5.सफेद मक्खियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- आक्रामक सफेद मक्खियाँ अपने बहुभक्षी प्रकृति और विपुल प्रजनन के कारण बढ़ रही हैं।
- सफेद मक्खी की अधिकांश प्रजातियाँ कैरिबियाई द्वीपों या मध्य अमेरिका की मूल निवासी हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
सफेद मक्खियाँ
- व्हाइटफ्लाइज़ छोटे, रस चूसने वाले कीड़े हैं जो सब्जी और सजावटी पौधों में प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं, खासकर गर्म मौसम के दौरान।
- वे चिपचिपे शहद का उत्सर्जन करते हैं और पत्तियों के पीलेपन या मृत्यु का कारण बनते हैं।
- पहली रिपोर्ट की गई आक्रामक सर्पिलिंग व्हाइटफ्लाई (एलेउरोडिकस डिस्पर्सस) अब जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में वितरित की जाती है।
- इसी तरह, 2016 में तमिलनाडु के पोलाची में रिपोर्ट की गई रगोज सर्पिलिंग व्हाइटफ्लाई (एलेउरोडिकस रगियोपरकुलैटस) अब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीपों सहित पूरे देश में फैल गई है।
- एलेरोडीकस डिस्पर्सस और एलेउरोडिकस रगियोपरक्यूलेटस को क्रमशः 320 और 40 से अधिक पौधों की प्रजातियों पर सूचित किया गया है।
- सभी आक्रामक सफेद मक्खियों की मेजबान सीमा उनकी बहुपक्षीय प्रकृति (विभिन्न प्रकार के भोजन पर भोजन करने की क्षमता) और विपुल प्रजनन के कारण बढ़ रही है।
- भारत में लगभग 1.35 लाख हेक्टेयर नारियल और ताड़ का तेल रगोज सर्पिलिंग व्हाइटफ्लाई से प्रभावित है।
- उपलब्ध सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग करके सफेद मक्खियों को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है।
- वे वर्तमान में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कीट परभक्षी, परजीवी (कीटों के प्राकृतिक शत्रु, ग्रीनहाउस और फसल के खेतों में कीटों का जैविक नियंत्रण प्रदान करते हैं) और एंटोमोपैथोजेनिक कवक (कवक जो कीड़ों को मार सकते हैं) द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं।
- व्हाइटफ्लाइज़ के लिए विशिष्ट एंटोमोपैथोजेनिक कवक अलग, शुद्ध, प्रयोगशाला में उगाए जाते हैं या बड़े पैमाने पर उत्पादित होते हैं और लैब-पाले संभावित शिकारियों और पैरासिटोइड्स की रिहाई के साथ संयोजन में व्हाइटफ्लाई पीड़ित क्षेत्र में लागू होते हैं।
Q 6.हाल ही में खबरों में रही नीलेश शाह समिति का संबंध किससे है?
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में निवेश कोष को बढ़ावा देना।
- भारत में चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने से।
- पूंजी बाजार अवसंरचना संस्थानों (MIIs) की कार्यप्रणाली से।
- इनमे से कोई भी नहीं।
ANSWER: 1
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में फंड उद्योग के लिए रोड मैप पर IFSCA की सिफारिश करने के लिए निवेश निधि पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
- समिति का गठन श्री नीलेश शाह, एमडी, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की अध्यक्षता में किया गया है।
- समिति में प्रौद्योगिकी, वितरण, कानूनी, अनुपालन और संचालन जैसे क्षेत्रों सहित पूरे फंड प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र के नेता शामिल हैं।
विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ विषय:
- IFSC में निवेश कोष के संचालन के लिए दीर्घकालिक दृष्टि पर IFSCA की सिफारिश करना।
- IFSC में निवेश कोष की संरचना के संबंध में सिफारिशें करने के लिए।
- अंतर-नियामक मुद्दों सहित IFSCs में निवेश निधि उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करना।
- एसेट मैनेजर्स, हेज फंड्स, पीई, वीसी, सॉवरेन फंड्स, फैमिली ऑफिस और उससे जुड़ी प्रोफेशनल सेवाओं के साथ-साथ इकोसिस्टम के निर्माण पर कोई अन्य प्रासंगिक आइटम।
Q 7.सुपरमून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
- यह तब होता है जब चंद्रमा की कक्षा/ऑर्बिट उसी समय पृथ्वी के सबसे करीब होती है जब चंद्रमा पूरा होता है।
- चंद्र पेरिगी तब होती है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकट होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- 26 मई को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट पहुंचेगा और इसलिए यह 2021 का सबसे निकटतम और सबसे बड़ा पूर्ण चंद्रमा या “सुपरमून” प्रतीत होगा।
- यह खगोलीय घटना इस साल के एकमात्र पूर्ण चंद्र ग्रहण के साथ मेल खाती है, जो जनवरी 2019 के बाद पहला है।
- गौरतलब है कि करीब छह साल में सुपरमून और पूर्ण चंद्रग्रहण की घटना एक साथ नहीं हुई है।
- सुपरमून तब होता है जब चंद्रमा की कक्षा/ऑर्बिट उसी समय पृथ्वी के सबसे करीब होती है जब चंद्रमा पूरा होता है।
- जैसे-जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तब एक समय ऐसा आता है जब दोनों के बीच की दूरी सबसे कम होती है (उसे पेरिगी कहा जाता है जब औसत दूरी पृथ्वी से लगभग 360,000 किमी होती है) और एक समय ऐसा आता है, जब दूरी सबसे अधिक होती है (उसे अपोजी कहा जाता है जब दूरी पृथ्वी से लगभग 405,000 किमी होती है)।
- अब, जब एक पूर्ण चंद्रमा उस बिंदु पर प्रकट होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम होती है, तो वह न केवल उज्जवल दिखाई देता है, बल्कि यह एक नियमित पूर्णिमा से भी बड़ा होता है।
- नासा के अनुसार, सुपरमून शब्द को 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोल ने गढ़ा था।
- एक सामान्य वर्ष में, दो से चार पूर्ण सुपरमून और लगातार दो से चार नए सुपरमून हो सकते हैं।
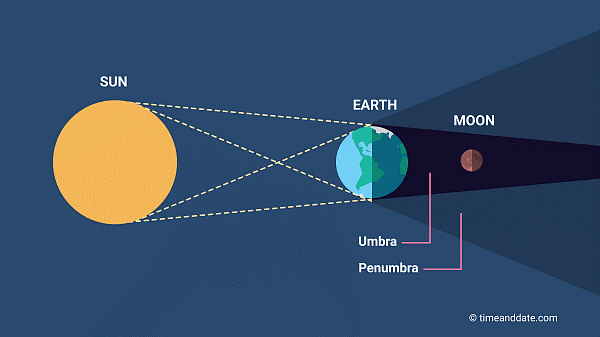
Q 8.मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं
- वे कृत्रिम रूप से निर्मित एंटीबॉडी हैं जिनका उद्देश्य शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता करना है।
- वे एक विशिष्ट एंटीजन को लक्षित करते हैं जो रोगज़नक़ से एक प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी
- वे कृत्रिम रूप से निर्मित एंटीबॉडी हैं जिनका उद्देश्य शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता करना है।
- वे एक विशिष्ट एंटीजन को लक्षित करते हैं जो रोगज़नक़ से एक प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है।
- एक विशेष प्रतिजन के लिए सफेद रक्त कोशिकाओं को उजागर करके प्रयोगशाला में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया जा सकता है।
- उत्पादित एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ाने के लिए, एक एकल श्वेत रक्त कोशिका का क्लोन बनाया जाता है, जिसका उपयोग एंटीबॉडी की समान प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है।
- कोविड -19 के मामले में, वैज्ञानिक आमतौर पर SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन के साथ काम करते हैं, जो मेजबान सेल में वायरस के प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है।
- एक स्वस्थ शरीर में, प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी बनाने में सक्षम होती है – हमारे रक्त में छोटे वाई-आकार के प्रोटीन जो माइक्रोबियल दुश्मनों को पहचानते हैं और उन्हें बांधते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को फिर रोगज़नक़ पर हमला शुरू करने का संकेत देते हैं।
- हालांकि, जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली इन एंटीबॉडी की पर्याप्त मात्रा में बनाने में असमर्थ हैं, उनके लिए वैज्ञानिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करने में मदद करते हैं।
- मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अब अपेक्षाकृत आम हैं, उनका उपयोग इबोला, एचआईवी, सोरायसिस आदि के इलाज में किया जाता है।
- इटोलिज़ुमैब और टोसीलिज़ुमैब दो महत्वपूर्ण दवाएं हैं जिनका उपयोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी में किया जाता है।
Q 9.हेट स्पीच/ द्वेषपूर्ण भाषण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- द्वेषपूर्ण भाषण को एक ऐसे भाषण के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति की पहचान और अन्य लक्षणों के आधार पर उन्हें बदनाम करने, अपमानित करने, धमकी देने या लक्षित करने के लिए होता है।
- टी.के. विश्वनाथन समिति का गठन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में सुधारों का सुझाव देने के लिए किया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2
ANSWER: 3
- ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में सुधारों का सुझाव देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित पैनल “भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित अपराधों” पर एक अलग धारा का प्रस्ताव कर सकता है।
- आईपीसी में “द्वेषपूर्ण भाषण” के लिए कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसलिए आपराधिक कानूनों में सुधार समिति पहली बार इस तरह के भाषण को परिभाषित करने का प्रयास कर रही है।
- उम्मीद है कि समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए समिति द्वारा प्राप्त सुझावों की जांच मंत्रालय द्वारा उन्हें अपनाने से पहले की जाएगी।
- ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने हाल ही में साइबर उत्पीड़न के मामलों पर जांच एजेंसियों के लिए एक मैनुअल प्रकाशित किया है, जिसमें द्वेषपूर्ण भाषण को “एक ऐसे भाषण के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति की पहचान और अन्य लक्षणों (जैसे यौन अभिविन्यास या विकलांगता या धर्म आदि) के आधार पर उन्हें बदनाम करने, अपमानित करने, धमकी देने या लक्षित करने के लिए होता है।”
विश्वनाथन समिति:
- इससे पहले 2018 में, गृह मंत्रालय ने एक समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन “द्वेषपूर्ण भाषण” के लिए एक अलग कानून तैयार करने के लिए विधि आयोग को लिखा था।
- इस समिति ने लोकसभा के पूर्व महासचिव टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में कड़े कानूनों की सिफारिश की थी।
- समिति का गठन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 ए के मद्देनजर किया गया था, जो संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिए दंड प्रदान करता था।
- इसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
Q 10.निम्नलिखित में से किन सिफारिशों पर बिमल जालान समिति ने आरबीआई को जोर दिया था ?
- विनिवेश नीति(Disinvestment policy)
- मौद्रिक नीति समिति(Monetary policy)
- अधिशेष वितरण नीति(Surplus delivery policy)
- पूंजी खाता परिवर्तनीयता(Capital convertability account)
ANSWER: 3
बिमल जालान समिति
- आरबीआई ने अपने आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करने और सरकार को हस्तांतरित किए जाने वाले अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा का सुझाव देने के लिए पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
- पैनल ने आरबीआई की आर्थिक पूंजी के दो घटकों यानी रियलाइज्ड इक्विटी और रिवैल्यूएशन बैलेंस के बीच स्पष्ट अंतर की सिफारिश की।
- पुनर्मूल्यांकन भंडार में विदेशी मुद्राओं और सोने, विदेशी प्रतिभूतियों और रुपया प्रतिभूतियों और एक आकस्मिक निधि के मूल्यों में आवधिक रूप से चिह्नित-से-बाजार अप्राप्त / काल्पनिक लाभ / हानि शामिल हैं।
- वास्तविक इक्विटी, जो मुख्य रूप से प्रतिधारित आय से निर्मित सभी जोखिमों / हानियों को पूरा करने के लिए एक आकस्मिक निधि का एक रूप है, इसे आकस्मिक जोखिम बफर (सीबीआर) भी कहा जाता है।
- आरबीआई की अधिशेष वितरण नीति जिसे अंतिम रूप दिया गया था, वह बिमल जालान समिति की सिफारिशों के अनुरूप है।
- जालान समिति ने आकस्मिक जोखिम बफर के लिए आरबीआई की बैलेंस शीट की 5.5-6.5% की सीमा दी है।
- सिफारिशों का पालन करते हुए, आरबीआई ने सीबीआर स्तर को बैलेंस शीट के 5.5% पर सेट करने का निर्णय लिया है।
अन्य समितियां
- विनिवेश नीति की सिफारिश जीवी रामकृष्ण समिति द्वारा की जाती है
- तारापुर समिति द्वारा पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश की जाती है
- मौद्रिक नीति समिति की सिफारिश उर्जित पटेल समिति द्वारा की जाती है